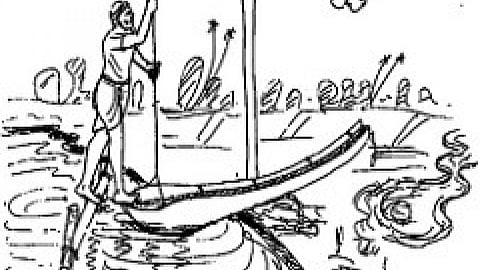भूमिगत जल संरक्षण - संचयन और कम पानी की सिंचाई विधियाँ
(Ground Water Conservation - Less Water Irrigation Methods)
कृषि विकास किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड है। सघन फसल उत्पादन में पानी एक अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण घटक है, जिसका कोई विकल्प नहीं है। वस्तुतः यह कटु सत्य है कि सम्पूर्ण विश्व में जल ही ऐसा संसाधन है, दो निरंतर चिंता का विषय बना हुआ है। वर्तमान में जल संकट के कई कारण है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, कम होती वर्षा का परिमाण, बढ़ता औद्योगिकीकरण, बढ़ता शहरीकरण, वृक्षों कि अंधाधुंध कटाई, विलासिता, आधुनिकतावादी एवं भोगवादी प्रवृत्ति, स्वार्थी प्रवृत्ति एवं जल के प्रति संवेदनहीनता, भूजल पर बढ़ती निर्भरता एवं इसका अत्यधिक दोहन, परम्परागत जल संग्रहण तकनीकों की उपेक्षा, समाज की सरकार पर बढ़ती निर्भरता, कृषि में बढ़ता जल का उपभोग आदि।
आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 22 मई 2016 को पानी बचाने, बारिश का पानी सहेजने और जल-सिंचन में मितव्ययता पर देर तक बात की। उन्होंने देश के लोगों से अपने मन की बात करते हुए इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री भी देश में व्याप्त जल संकट से चिंतित नजर आए। उन्होंने देश में कई जगह पानी को लेकर किये जा रहे अच्छे कामों की सराहना करते हुए देशवासियों से आग्रह किया कि अभी अच्छी बारिश आने तक चार महीनों हम सबको पानी के लिये काम करने का समय है। हमें बारिश की हर बूँद को सहेजना है।
जल संचयन
वर्षा का ज्यादातर पानी सतह की सामान्य ढालों से होता हुआ नदियों में जाता है तथा उसके बाद सागर में मिल जाता है। वर्षा के इस बहुमूल्य शुद्ध जल का भूमिगत जल के रूप में संरक्षण अति आवश्यक है। भूमिगत जल कुएँ, नलकूप आदि साधनों द्वारा खेती ओर जनसामान्य के पीने हेतु काम आता है।
भूमिगत जल, मृदा (धरती की उपरी सतह) की अनेक सतहों कि नीचे चट्टानों के छिद्रों या दरारों में पाया जाता है। उपयोगिता कि दृष्टि से भूमिगत जल, सतह पर पीने योग्य उपलब्ध जल संसाधनों के मुकाबले अधिक महत्त्वपूर्ण है। भारत के लगभग अस्सी प्रतिशत गाँव, कृषि एवं पेयजल के लिये भूमिगत जल पर ही निर्भर हैं और दुश्चिंता यह है कि विश्व में भूमिगत-जल अपना अस्तित्व तेजी से समेट रहा है। अन्य विकासशील देशों में तो यह स्थिति भयावह है ही, जहाँ जलस्तर लगभग तीन मीटर प्रति वर्ष की रफ़्तार से कम हो रहा है, पर भारत में भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं।
केन्द्रीय भूजल बोर्ड के अन्वेषणों के अनुसार भारत के भूमिगत जल स्तर में 20 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की औसत दर से कमी हो रही है, जो हमारी भीमकाय जनसंख्या ज़रूरतों को देखते हुए गहन चिंता का विषय है।
ना तो हर प्रकार की मिट्टी, पानी को जलग्रहण करने वाले इन चट्टानों तक पहुँचाने में सक्षम होती है और न ही हर प्रकार की चट्टानें पानी को ग्रहण कर सकती हैं। कायांतरित अथवा आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा अवसादी चट्टानें अधिक जलधारक होती हैं, जैसे कि बलुआ चट्टानें। कठोर चट्टानों में जल-संग्रहण कर सकने योग्य छिद्र ही नहीं होते। हाँ यदि ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थरों ने किसी कारण दरारें उत्पन्न हो गयी हों तो वो भी भूमिगत जल को स्वयं में संग्रहण करती हैं। जिन भूमिगत चट्टानों में छिद्र अथवा दरारें होती हैं, उनमें यह पानी न केवल संग्रहित हो जाता है, अपितु एक छिद्र से दूसरे छिद्र होते हुए अपनी हलचल भी बनाये रखता है, और ऊँचे से निचले स्थान की ओर प्रवाहित होने जैसे सामान्य नियम का पालन भी करता है। मृदा से चट्टानों तक पहुँचने की प्रक्रिया में पानी छोटे-बड़े प्राकृतिक छिद्रों से छनता हुआ संग्रहित होता है, अतः इसकी स्वच्छता निर्विवाद है। किन्तु यही पानी यदि प्रदूषित हो जाये तो फिर बहुत बड़े जल-संग्रहण को नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि ये भूमिगत जलसंग्रह बड़े या आपस में जुड़े हो सकते हैं।
वर्षाजल और सतही जल का आपसी संबंध भी जानना आवश्यक है। नदियों में बहने वाला जल केवल वर्षाजल अथवा ग्लेशियर से पिघल कर बहता हुआ पानी ही नहीं हैं। नदी अपने जल में भूमिगत जल से भी योगदान लेती है, साथ ही भूमिगत जल को योगदान देती भी है। ताल, झील और बाँधों के इर्द-गिर्द भूमिगत जल की सहज सुलभता का कारण यही है कि ये ठहरे हुए जलस्रोत आहिस्ता-आहिस्ता अपना पानी इन भूमिगत प्राकृतिक जल संग्रहालयों को प्रदान करते रहतेे हैं। इस प्रकार पृथ्वी के उपर पाए जाने वाले जलस्रोत और भूमिगत जलस्रोत एक दूसरे की सहायता पर निर्भर होते हैं। वर्षा का जल यदि संग्रहित कर चट्टानों तक पहुँचाया जाये तो भूमिगत जलाशयों को भरा जा सकता है। प्रकृति अपने सामान्य क्रम में यह कार्य करती रहती हैं। किंतु आज जब यह समस्या विकराल रूप ले चुकी है, तो मनुष्य के लिये अभियान बनाकर यह कार्य करना आवश्यक हो गया है। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य जल को जीवन मान कर बचाया जाना और सरल वैज्ञानिक विधियों द्वारा इसे भूमि के भीतर पहुँचाया जाना है,जिसमें हम सभी को जुटना होगा।
भूमिगत जल के संचयन एवं संरक्षण हेतु प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर निम्न कार्य अवश्य ही करना चाहिएः
1. वर्षाकाल में मकानों की छत पर गिरे जल को जमीन में पहुँचाने की व्यवस्था बना दी जाए।
2. आंगन को कच्चा रखने की पुरानी परंपराओं का पालन किया जाए।
3. कम से कम एक वृक्ष लगाया जाए।
4. पानी की बर्बादी को रोका जाए, जैसे कि उपयोग के बाद नल को बंद कर दिया जाए।
5. सरकारी प्रयास और वैज्ञानिक शोधों से इस समस्या का आंशिक समाधान ही निकलेगा, किंतु यदि सामान्यजन इस बात को समझ लें, तो बूँद-बूँद से धड़ा भरते देर नहीं लगेगी।
बूँद-बूँद से घड़ा भरता है और बारिश के पानी से भूगर्भ जल का स्तर ऊंचा होता है। आकाशीय पानी को भूगर्भ स्रोत से जोड़ने के लिये जगह-जगह पर रिचार्ज-पिट की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि-अतिवृष्टि में भी पानी बह कर बर्बाद नहीं हो। वर्षा-जल संधारण जरूरी भी है और जिम्मेदारी भी है।
कम पानी की सिंचाई पद्धतियाँ
वैज्ञानिकों ने निरंतर अनुसंधान द्वारा ऐसी सिंचाई विधियाँ विकसित की हैं, जिनसे पानी व उर्जा की न केवल बचत होती है, वरन, कृषि उपज भी अधिक प्राप्त होती है। ये पद्धतियाँ हैं- फव्वारा एवं बूँद-बूँद सिंचाई प्रणाली।
फव्वारा एवं बूँद-बूँद सिंचाई पद्धतियों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पानी का ह्रास नहीं होता, क्योंकि पानी पाइप द्वारा प्रवाहित होता है तथा फव्वारा या बूँद-बूँद रूप में दिया जाता है। इन पद्धतियों से 75 से 95 प्रतिशत तक पानी खेत में फसल को मिलता है, जबकि प्रचालित सतही विधियों में 40 से 60 प्रतिशत ही फसल को मिल पाता है। इतना ही नहीं फव्वारा एवं बूँद-बूँद सिंचाई पद्धतियों की खरीद पर सरकार 50 से 75 प्रतिशत तक अनुदान भी देती है।
फव्वारा पद्धति
इस पद्धति में पानी पाईप व फव्वारों द्वारा वर्षा के रूप में दिया जाता है। यह विधि असमतल भूमि के लिये अति उपयुक्त है। यह विधि 2 से 10 किग्रा./सेमी., दाब पर काम करती है। नोजल का व्यास 1.5 मिमी. से 40 मि.मी. तक होता है। इनसे 1.5 लीटर/सेकेंड से 50 लीटर/सेकेंड की दर से पानी फव्वारे के रूप में निकलता है। एक फव्वारे द्वारा 6 से 160 मीटर तक क्षेत्रफल सिंचित किया जा सकता है। हमारे देश में बहुधा 6 से 15 मीटर की दूरी तक पानी छिड़कने के सिंचाई फव्वारे उपलब्ध है। इन्हें चलाने के लिये 2,5 किग्रा, प्रति सेमी2,दबाव की जरूरत होती है। यह विधि बाजरा, गेहूँ, सरसों व सब्जियों के लिये अति उपयुक्त पाई गई है। कम लवणीय जल होने पर भी यह विधि उपयोग में लाई जा सकती है, परंतु अधिक लवणीय जल होने पर यह अनुपयुक्त है। इस विधि द्वारा नाइट्रोजन उर्वरक, कीट एवं कवक-नाशक दवाइयों का भी छिड़काव किया जा सकता है।
बूँद-बूँद सिंचाई
| तालिका-1ः बूँद-बूँद सिंचाई द्वारा विभिन्न फसलों में पानी की बचत व पैदावार | ||||
| फसल | प्रचलित विधि | बूँद-बूँद सिंचाई विधि | ||
| पानी की मात्रा (मि.मी.) | पैदावार (टन/हे.) | पानी की मात्रा (मि.मी.) | पैदावार (टन/हे.) | |
| लाल मिर्च | 1184 | 1.93 | 813 | 2.94 |
| टमाटर | 700 | 50 | 350 | 90 |
| फूलगोभी | 240 | 20 | 120 | 26 |
| पत्तागोभी | 240 | 25 | 120 | 33 |
| शलगम | 200 | 16 | 100 | 23 |
| आलू | 490 | 20 | 350 | 30 |
| मक्का | 558 | 6 | 360 | 12 |
तालिका 1 में बूँद-बूँद सिंचाई द्वारा विभिन्न फसलों में पानी का बचत व पैदावार का विवरण दिया गया है, जिससे विदित होता है कि इस पद्धति से 30 से 50 प्रतिशत तक पानी की बचत व ड़ेढ से दो गुना अधिक पैदावार मिलती है। बूँद-बूँद सिंचाई थोड़ी महंगी है। अतः दो पंक्तियों के बीच एक ड्रिप लाइन 1.20 से 1.50 मीटर की दूरी पर डालने से 50 प्रतिशत खर्चा कम किया जा सकता है। इस विधि द्वारा लवणीय पानी भी सब्जियों में दिया जा सकता है।
सिंचाई की कोई भी विधि क्यों न हो, वाष्पोत्सर्जन की अपेक्षा वाष्पीकरण की हानि कम होनी चाहिए। पानी इस तरह से देना चाहिए, जिससे अंतः भूमि सतह में कटाई के समय पानी न के बराबर रहे। इसी प्रकार सिंचाई जल की मात्रा इतनी भी ज्यादा न रहे कि भूमि की अंतः सतह में पानी चला जाए।
उपयुक्त वर्णित सिंचाई प्रबंधन से हम प्रति इकाई पानी से अधिक पैदावार ले सकते हैं अपने जल स्रोतों को लम्बे समय तक प्रयोग में ले सकते हैं। इसके साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं। हमारा दूसरी हरित क्रांति का सपना पानी का सदुपयोग करने से ही पूरा होगा।
लवणीय जल से भी सिंचाई की जा सकती है, इसको उपयुक्त बनाने के कुछ सुझाव दिए गए है, जिन्हें अपनाकर किसान भाई उपज में लाभ प्राप्त कर सकते हैं -
1. लवण सहनशील फसलें, जैसे- गेहूँ, बाजरा, जौ, पालक, सरसों आदि का अधिक उपयोग करें।
2 . संचाई करते समय फव्वारा एवं बूँद-बूँद सिंचाई प्रणाली को अपनाएँ।
3. जल निकास की समुचित व्यवस्था रखें एवं हरी खाद का अधिक प्रयोग करें ।
4. वर्षा के समय खेत में मेंड़बंदी कर वर्षा के पानी को एकत्रित करें, जिससे लवण धुलकर बाहर आ जाएँगे।
5. सिंचाई की संख्या बढ़ाएँ तथा प्रति सिंचाई कम मात्रा में जल का प्रयोग करें।
6. यदि पीने योग्य पानी की अच्छी सुविधा उपलब्ध है, तो लवणीय जल तथा मीठे जल दोनों को मिलाकर भी सिंचाई की जा सकती है।
अतः आशा की जाती है कि किसान भाई वर्षाजल का भू-जल के रूप में संचयन करते हुए सिंचाई की उन्नत विधियों को अपनाकर कृषि में हो रहे जल अपव्यय को रोक सकते हैं।