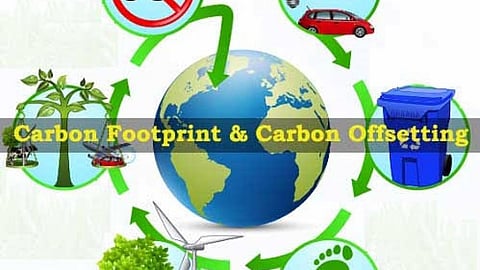ताकि न रहे कार्बन फुटप्रिंट का नामोनिशान
टी वी रामाचन्द्र, भरत सेत्तुर, विनायक एस, भरत एच ऐथल, योजना, जनवरी, 2020
पेरिस में हुए जलवायु परिवर्तन समझौते में भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33-35 प्रतिशत कमी करने का वादा किया था जिसके लिए जरूरी है कि परती भूमि पर तत्काल स्थानीय प्रजातियों के पेड़-पौधे लगाकर ‘कार्बन कैप्चर’ को तत्काल कम किया जाए, भूमि के उपयोग और भूमि के आच्छादन का विनियमन किया जाए और नवीकरणीय और चिरस्थाई ऊर्जा विकल्पों का बड़े पैमाने पर उपयोग करके डीकार्बनाइजेशन यानी कार्बनमुक्त करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। इस लेख में पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील पश्चिमी घाट क्षेत्र की मिसाल लेकर इस विषय का गहराई से अध्ययन किया गया है।
ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती के तापमान में असामान्य वृद्धि और मानवजनित ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बेतहाशा बढ़ने से लोगों की आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। औद्योगिक युग से पहले कार्बन डाइऑक्सइड का उत्सर्जन 280 पीपीएम था, जो आज 400 पीपीएम के स्तर पर पहुँच गया है। इसके परिणामस्वरूप जलवायु में बदलाव आया है, पारिस्थितिकीय प्रणाली की उत्पादकता गिरी है और पानी का आधार घट गया है। मानवजनित गतिविधियों जैसे बिजली के उत्पादन, कृषि और उद्योग आदि में जीवाश्म ईंधन जलाने, पानी के स्रोतों के प्रदूषित होने और शहरी गतिविधियों से धरती के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा 72 प्रतिशत के बराबर है। पारिस्थितिकीय प्रणाली की गतिविधियों को बरकरार रखने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइ ऑक्साइड का अवशोषण कर ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति को संतुलित करना जरूरी हो गया है। कार्बन को अवशोषित करने में वनों की बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका है और वे करीब 45 प्रतिशत कार्बन को अवशोषित कर ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम करने में मदद करते हैं।
भूमि उपयोग भूमि आच्छादन की प्रक्रिया से वनों का ह्रास होता है और जमीन का खराब होना ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जन होता है और कार्बन क्षमता में गिरावट आती है। पश्चिमी घाट जैव विविधता के 36 वैश्विक केन्द्रों में से एक हैं और इस क्षेत्र के वन वायुमंडलीय कार्बन का अवशोषण करते हैं जिससे दुनिया की जलवायु को सामान्य बनाए रखने में मदद मिलती है। इस क्षेत्र में 4,600 प्रजातियों के फूलवाले पौधे पाए जाते हैं (38 प्रतिशत स्थानिक), 330 प्रकार की तितलियां (11 प्रतिशत स्थानिक), 156 सरीसृप (62 प्रतिशत स्थानिक), 508 पक्षी (4 प्रतिशत स्थानिक) 120 स्तनपाई (12 प्रतिशत स्थानिक), 289 मछलियां (41 प्रतिशत स्थानिक) और 135 उभयचर (75 प्रतिशत स्थानिक) पाई जाती हैं। यह क्षेत्र 1,60,000 वर्ग किमी. में फैला हुआ है और इसे भारत का वाटर टावर माना जाता है क्योंकि अनेक धाराएं यहाँ से निकलती हैं और लाखों हेक्टेयर भूमि से जल की निकासी करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों के 24.5 करोड़ लोगों को पानी और भोजन की सुरक्षा उपलब्ध कराती हैं। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के साथ-साथ आर्द्र पर्णपाती वन, झाड़ीदार वन, वनखंड और सामान्य व अत्यधिक वर्षा वाले सवाना वन हैं जिसमें से 10 प्रतिशत वन क्षेत्र ही कानूनी संरक्षण के अन्तर्गत है।
भूमि उपयोग के तौर-तरीकों का आकलन लैंडसैट 8 ऑपरेशन लैंड इमेजर (ओएलआई-30 एम रिजॉल्यूशन) 2018 के पृथ्वी सम्बन्धी दूर संवेदन आंकड़ों से किया गया और उन्हें क्षेत्रीय अनुमानों और इंटरनेशनल जीओस्फेयर-बायोस्फेयर कार्यक्रम (आईजीबीपी) से उपलब्ध दशकीय भूउपयोग अनुमानों (1985, 1995, 2005-100 मीटर रिजॉल्यूशन) के साथ समन्वित किया गया। इस तरह समन्वित किए गए आनुषंगिक आंकड़ों में आंकलन के फ्रेंच संस्थान द्वारा बनाए गए वनस्पति मानचित्र, उष्मकटिबंधीय मानचित्र (सर्वे ऑफ इंडिया) और वर्चुअल अर्थ डेटा (गूगल अर्थ, भुवन) को भी लिया गया था। वनों की पारिस्थितिकीय प्रणाली की कार्बन अवशोषित करने की क्षमता का आकलन (1) मानक बायोमास परीक्षणों पर आधारित लिखित साहित्य; और (2) कर्नाटक के पश्चिमी घाट वाले इलाके के वनों से ट्रांसेक्ट आधारित क्वाड्रेंट सैम्पलिंग तकनीक से एकत्र किए गए क्षेत्र आधारित मापनों से किया गया।
चित्र 1:
चित्र 1 में दिए गए भू-अंतरिक्ष भूमि उपयोग विश्लेषण से मानवीय दबाव से वन क्षेत्र के नुकसान का पता चलता है। इस क्षेत्र में 1985 में 16.21 प्रतिशत क्षेत्र में सदाबहार वन थे जो 2018 में 11.3 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिमट कर रह गए। यहां क्रमशः 17.92 प्रतिशत, 37.53 प्रतिशत, 4.88 प्रतिशत क्षेत्र बागान, कृषि, खनन और निर्मित इलाके के अन्तर्गत है। भू-उपयोग में बदलाव मोनोकल्चर यानी एक ही प्रकार के बागान, जैसे अकेशिया, यूकेलिप्टस, साल और रबड़ लगाने, विकास परियोजनाओं और कृषि विस्तार के कारण हुआ है। 1983 से 2018 के दौरान इस क्षेत्र में आस-पास के अंदरूनी क्षेत्र में वन आच्छादन नष्ट हुआ है जबकि वनेतर आच्छादन में बढ़ोत्तरी (11 प्रतिशत) हुई है। इस इलाके में अंदरूनी वन (जो 2018 में 25 प्रतिशत क्षेत्र में थे) प्रमुख संरक्षित क्षेत्र में हैं और लगातार बढ़ते मानवीय दबाव की वजह से सीमांत वन अधिक महत्त्वपूर्ण होते जा रहे हैं। (चित्र 2)। गोवा में अंधाधुंध खनन गतिविधियों की वजह से अंदरूनी वनाच्छादित क्षेत्र की बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। 2031 के अनुमानित भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र और निर्मित क्षेत्र में क्रमश: 39 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का पता चलता है। पश्चिमी घाट के पूर्वी केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कृषि और निर्मित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलावों को देखा जा सकता है। अनुमान है कि पश्चिमी घाट में 2031 तक सदाबहार वन क्षेत्र सिमट कर 10 प्रतिशत ही रह जाएगा जिससे पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा इसका असर प्रायद्वीपीय भारत के लोगों की खाद्य सुरक्षा और आजीविका पर पड़ने की आशंका है।
कार्बन अवशोषण
पश्चिमी घाट की कार्बन अवशोषण क्षमता का मात्रात्मक आंकलन कर लिया गया है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र के वन बायोमास के अनोखे भंडार हैं। यह आकलन वायुमंडलीय कार्बन (मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न) और ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम करने में वनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है। पश्चिमी घाट के दक्षिणी और मध्यवर्ती भागों में घने स्थानीय वन हैं और यहाँ की भूमि कार्बन से समृद्ध है (0.42 एमजीजी)। इसी तरह का रुझान मिट्टी में वृद्धिशील कार्बन अवशोषण में भी देखा गया है जिसमें इसकी मात्रा 15120 जीजी और पश्चिमी घाट के कर्नाटक तथा मध्यवर्ती केरल वाले इलाके में वार्षिक कार्बन वृद्धिशीलता के ऊंचे स्तर पर है। अगर उत्पादकता के जरिए होने वाली कार्बन क्षति को छोड़ दिया जाए तो कुल वृद्धिशील कार्बन की मात्रा 37507.3 जीजी बैठती है। पश्चिमी घाट में कार्बन अवशोषण क्षमता में होने वाले बदलाव का आंकलन भूमि उपयोग (1) संरक्षण परिदृश्य और (2) रोजमर्रा की गतिविधियों के परिदृश्य में भूमि संभावित उपयोग के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। रोजमर्रा की गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने से (जिसमें भूमि उपयोग में बदलाव से वनाच्छादित क्षेत्र में कमी का वर्तमान रुझान है) धरातल पर 1.3 एमजीजी के बायोमास पता चलता है जिसमें भंडारित कार्बन 0.65 एमजीजी और मृदा कार्बन 0.34 एमजीजी है।
कार्बन फुटप्रिंट
भारत में जहाँ कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जन 3.1 एमजीजी (2017) और प्रति व्यक्ति कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जन 2.56 मीट्रिक टन के बराबर है और यहाँ के कार्बन फुटप्रिंट में ऊर्जा क्षेत्र (68 प्रतिशत), कृषि क्षेत्र (19.6 प्रतिशत), औद्योगिक प्रकियाओं के (6 प्रतिशत) और भूमि के उपयोग में बदलाव (3.8 प्रतिशत) से होने वाले उत्सर्जन तथा वानिकी (1.9 प्रतिशत) का योगदान है। भारत के प्रमुख महानगरों में ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि, पशुधन प्रबंधन और अपशिष्ट क्षेत्र का वार्षिक कार्बन उत्सर्जन करीब 1.3 एमजीजी के बराबर है जिसमें दिल्ली (38633.20 जीजी), ग्रेटर मुम्बई (22783.08 जीजी), चेन्नई (22090.55 जीजी), बंगलुरु (19796.6 जीजी), कोलकाता (14812.1 जीजी), हैदराबाद (13734.59 जीजी) और अहमदाबाद (6580.4 जीजी) है।
पारिस्थतिकीय दृष्टि से नाजुक पश्चिमी घाट कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनमें सभी दक्षिण भारतीय शहरों से होने वाले कार्बन डाइ ऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता है। यहीं नहीं ये भारत के कुल कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जन का 1.62 प्रतिशत अवशोषित कर सकते हैं। पश्चिमी घाट के राज्यों से कुल उत्सर्जन 352922.3 जीजी (टेबल 1) था और इनके जंगलों में 11 प्रतिशत उत्सर्जन अवशोषित करने की क्षमता है जो कार्बन कम करके जलवायु को सामान्य बनाने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। भारत ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता वार्ता में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33-35 प्रतिशत कमी करने की वचनबद्धता व्यक्ति की थी। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि कार्बन कैप्चर पर तत्काल अमल किया जाए। इसके लिए उजड़े हुए जंगलों के स्थान पर स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाए जाने चाहिए और भूमि उपयोग और भूमि आच्छादन सम्बन्धी विनियमों में बदलाव किए जाएं। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा और चिरस्थाई ऊर्जा विकल्पों पर बड़े पैमाने पर अमल करके कार्बन मुक्ति का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए (1) पारिस्थितिकी की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों की हिफाजत की जानी चाहिए; (2) ‘प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे’ के सिद्धान्त के अनुसार लगातार ज्यादा उत्सर्जन करने वालों को हतोत्साहित किया जाए (3) क्लस्टर आधारित विकेन्द्रित विकास दृष्टिकोण लागू किया जाए, और (4) उत्सर्जन में कमी के लिए प्रोत्साहन दिए जाएं। कार्बन ट्रेडिंग की अवधारणा ने कार्बन को अवशोषित करने की भारतीय वनों की क्षमता के महत्व को मौद्रिक रूप में साबित कर दिया है। पश्चिमी घाट के वनों की पारिस्थितिकीय प्रणाली 30 डॉलर प्रति टन की दर से 100 अरब रुपए मूल्य (1.4 अरब डॉलर) की है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली और सहभागियों की भागीदारी को सुचारु बनाने से वनों का दुरुपयोग काफी हद तक कम हो जाएगा र किसानों को पेड़ लगाने तथा दूसरे बेहतरीन उपयोग के लिए जमीन का इस्तेमाल करने की प्रेरणा मिलेगी।
टेबल 1 - पश्चिमी घाट के राज्यों में कार्बन उत्सर्जन | ||||||
राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश | उत्सर्जन (जीजी) प्रति वर्ष | कुल (जीजी)
| कार्बन की कमी की गई (जीजी) प्रति वर्ष
| प्रतिशत कमी | ||
CH (C02 समतुल्य | CO(C02 समतुल्य) | CO2 | ||||
| गोवा | 233 | 337 | 3881 | 4451 | 872 | 20 |
| गुजरात | 15546 | 14498 | 79138 | 109182 | 1947 | 2 |
| कर्नाटक | 15662 | 15239 | 54337 | 85237 | 10401 | 12 |
| केरल | 3167 | 6108 | 26047 | 35321 | 7617 | 22 |
| महाराष्ट्र | 23129 | 26497 | 105260 | 154886 | 11020 | 7 |
| तमिलनाडु | 15761 | 19190 | 71107 | 106058 | 5375 | 5 |
| दादर और नागर हवेली | 46 | 63 | 1458 | 1567 | 601 | 38 |
| कुल उत्सर्जन (जीजी) | 496703 | 37833 | 8 | |||
निरंतरता पर आधारित और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जल और खाद्य सुरक्षा
पारिस्थितिकीय दृष्टि से नाजुक पश्चिमी घाट अपनी बारहमासी नदी-नालों से प्रायद्वीपीय भारत की पानी की आवश्यकता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जलग्रहण क्षेत्रों में भूदृश्य सम्बन्धी बदलाव का असर पानी की सम्पूर्ण व्यवस्था पर पड़ता है जिससे जलवैज्ञानिक परिस्थितियों में परिवर्तन होते हैं जैसा कि बारहमासी और मौसमी नदी-नालों से स्पष्ट हो जाता है। पश्चिमी घाट के वनाच्छादित जलग्रहण क्षेत्रों में बारहमासी नदी-नाले पाए जाते हैं जबकि उजड़े हुए वनों वाले इलाकों में मौसमी नदी-नाले ही पाए जाते हैं। नदी-नाले बारहमासी तब होते हैं जब जलग्रहण क्षेत्रों के 60 प्रतिशत से ज्यादा इलाके में देशी प्रजातियों के पेड़-पौधे हों। इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसे इलाकों में जमीन छिद्रयुक्त होती है जिससे रिसकर पानी जमीन में समा जाता है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव पेड़-पौधों की जड़ों के सम्पर्क में आते हैं और सरंध्र मिट्टी पोषक तत्वों को पेड़-पौधों तक पहुंचाने में मदद करती है। बारहमासी और मौसमी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों की मिट्टी में सबसे अधिक आर्द्रता पाई जाती है। (61.47 से 61.57 प्रतिशत) और इसमें पोषक तत्व (कार्बन, नाइट्रोजन और पोटेशियम) पाए जाते हैं तथा इसका सामूहिक घनत्व भी कम होती है (0.50 से 0.57 ग्राम/घन सें.मी.)। दूसरी ओर मौसमी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र की मिट्टी का सामूहिक घनत्व अधिक होता है और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी कम (0.87 से 1.53 ग्राम/ घन से.मी.) पाई जाती है। इस विश्लेषण से देशी प्रजातियों वाले वनों की स्थानीय लोगों की जरूरत पूरा करने के साथ ही जलवैज्ञानिक व्यवस्था को बनाए रखने में भूमिका के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यह सम्बन्धित सरकारी एजेंसियों द्वारा जलग्रहण क्षेत्र (जलसंभर/नाले) के प्रबंधन के लिए भी बहुत जरूरी है। खंडित अभिशासन और पारिस्थितिकीय नैतिकता में गिरावट के साथ ही नीति सम्बन्धी निर्णय लेने वालों में दूरदर्शिता का अभाव वनों के उजड़ने और जमीन के खराब होने की मुख्य वजह हैं।
जनता की आजीविका के मिट्टी, पानी और इसकी उपलब्ध के तुलनात्मक मूल्यांकन से पता चलता है कि सूखे मौसम में मौसमी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में देशी प्रजातियों के पेड़-पौधों की अधिकता होने से (60 प्रतिशत से अधिक) मिट्टी में नमी और भूमिगत जल का स्तर अधिक हो जाता है। सभी मौसमों में पानी उपलब्ध रहने से मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ जाने से किसान अधिक आर्थिक फायदा देने वाली वाणिज्यिक फसलों की खेती कर सकते हैं जबकि दूसरे किसानों को कम वर्षा वाले मौसम में जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इससे जलग्रहण क्षेत्र में स्थानी प्रजातियों के पेड़-पौधे लगाने की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर देशी पेड़ पौधों के संरक्षण के प्रयासों की आवश्यकता भी रेखांकित होती है क्योंकि इससे स्थानीय लोगों की आजीविका और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
बागानी फसलें (जैसे सुपारी, नारियल, केला, पान के पत्ते और काली मिर्च) बारहमासी नदियों और नालों के जलग्रहण क्षेत्र में रहने वालों को आमदनी दिलाने वाले प्रमुख उत्पाद हैं। बागानी फसलों से 2009-10 में सालाना कुल 3,11,701 रुपए प्रति हेक्टेयर की सकल औसत आमदनी हुई जबकि औसत खर्च 37,034 रुपए प्रति हेक्टेयर वार्षिक रहा ( जो कि मुख्य रूप से बागान के रखरखाव पर खर्च हुआ) इससे सालाना 2,76,558 हेक्टेयर की आय हुई।
दूसरी ओर मौसमी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में (जहाँ बागानी फसलों के साथ-साथ धान की खेती को भी आमदनी की गणना में शामिल किया गया था) औसत सकल सालाना आमदनी 1,50,679 रुपए रही जबकि खर्च 6474.10 हेक्टेयर वार्षिक रहा जो रखरखाव और खेत तैयार कराने पर खर्च किया गया। इससे इस बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि नदियों में पानी का बने रहने से क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है जो जलग्रहण क्षेत्र में भूमि उपयोग के तौर-तरीकों (वनाच्छादित आवरण) पर निर्भर है। इस तरह जलग्रहण क्षेत्र के सही रहने की सामाजिक और पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के ले पानी की उपलब्धता बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यह बात बारहमासी नदी-नालों के जलग्रहण क्षेत्र में देशी पेड़-पौधों और वनस्पतियों के पाए जाने से स्पष्ट हो जाती है। इस तरह जलग्रहण क्षेत्रों में देशी प्रजातियों के पेड़-पौधों और वनस्पतियों का होना जलवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अहमियत रखता है क्योंकि नदी में स्थाई रूप से पानी की उपलब्धता का सीधा सम्बन्ध पर्यावरण से है।
इससे नदी के जलग्रहण क्षेत्रों के कुप्रबंधन के बोलबाले, वनों के नष्ट होने में तेजी, फसलें उगाने के गलत तौर-तरीकों और पानी के उपयोग में दक्षता के अभाव वाले आज के युग में नदी नाले प्रबंधन में समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। हमारा जोर बाकी देशी जंगलों के संरक्षण पर होना चाहिए जो जल सुरक्षा (बारहमासी नदियों) खाद्य सुरक्षा (जैव विविधता बनाए रखने) के लिए बहुत जरूरी हैं। उजड गए प्राकृतिक वनों को फिर से हरा-भरा करने का अब भी एक मौका है। इसके लिए संरक्षण और प्रबंधन के उचित तौर-तरीकों को अपनाना होगा। 20वीं सदी के नीति निर्धारकों के तौर तरीकों को वर्तमान में अपनाने से जलग्रहण क्षेत्रों की पानी को सहेज कर रखने की क्षमता में कमी आई है।
इससे पानी का भीषण संकट उत्पन्न हुआ है जो कि पिछले तीन साल से देश के 180 से 279 जिलों के लगातार सूखे की चपेट में आने से देखा जा सकता है। औसत तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी और पश्चिमी घाटों में बरसात के मौसम के दिनों के कम होने से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु के लिए आसन्न संकट का पता चलता है। इसका कारण जंगलों का काटा जाना या डीकार्बनाइजेशन यानी कार्बनमुक्त करने की प्रणाली में कमी आने से कार्बन फुटप्रिंट में हुई बढ़ोत्तरी है।
1,60,000 वर्ग किलोमीटर विस्तार वाले पश्चिमी घाट भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र (3,287,263 वर्ग कि.मी.) का केवल 4.86 प्रतिशत हैं और पश्चिमी घाट का करीब 1.94 प्रतिशत (64,000 वर्ग कि.मी.) क्षेत्र पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील है जो प्रायद्वीपीय भारत के 100 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें उगाने के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में हाल में बाढ़ और उसके बाद सूखे (पानी के स्रोतों के सूखना) क्षेत्र के जंगलों के कुप्रबंधन की ओर संकेत करता है।
इस क्षेत्र में संक्षिप्त अवधि में अधिक वर्षा हुई और जलग्रहण क्षेत्र की पानी का अवशोषण कर अपने में रोक कर रखने की क्षमता के खत्म हो जाने से (वनों के नष्ट होने से) वर्षा का ज्यादातर पानी जमीन के ऊपर से बहता हुआ समुद्र में चला गया जिससे बरसात के मौसम के तुरन्त बाद पानी की कमी पैदा हो गई। इसके अलावा जमीन धंसने जैसी घटनाओं से जान-माल का नुकसान भी हुआ। इसलिए पशिचमी घाट जैसे पारिस्थितिकी की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर संरक्षित करना जरूरी है ताकि प्रायद्वीपीय भारत में कृषि और बागवानी को बनाए रखा जा सके और स्वस्थ नागरिकों वाले विकासशील देश के दर्जे को हासिल करने के लिए 2025 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का भी निर्माण किया जा सके। जमीन, जंगल और पानी माफियाओं द्वारा थोपी गई एक तरफा विकास की नीतियों से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था खोखली हो जाएगी और बार-बार बाढ़ व सूखे की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
प्रकाशन विभाग विक्रय केन्द्र | |||
| नई दिल्ली | पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड | 110003 | 011-24367260 |
| दिल्ली | हाल सं. 196, पुराना सचिवालय | 110054 | 011-23890205 |
| नवी मुम्बई | 701, सी-विंग, सातवीं मंजिल, केन्द्रीय सदन, बेलापुर | 40014 | 022-27570686 |
| कोलकाता | 8, एसप्लानेड ईस्ट | 700069 | 033-22488030 |
| चेन्नई | ‘ए’ विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर | 600090 | 044-24917673 |
| तिरुअनंतपुरम | प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट | 695001 | 0471-2330650 |
| हैदराबाद | कमरा सं, 204 , दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद | 500080 | 040-27535383 |
| बंगलुरु | फर्स्ट प्लोर, ‘एफ’ विंग, केन्द्रीय सदन, कोरामंगला | 560034 | 080-25537244 |
| पटना | बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ | 800004 | 0612-2683407 |
| लखनऊ | हॉल सं-1, दूसरा तल, केन्द्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज | 226024 | 0522-2325455 |
| अहमदाबाद | पीआईबी, अखंडानंद हॉल, तल-2 मदर टेरेसा रोड, सीएनआई चर्च के पास, भद्र | 380001 | 079-26588669 |
सन्दर्भ
- रामाचंद्रा, टीवी, और भारत एस. (2019 ए) कार्बन सेक्वेस्टरेशन पोटेंशियल ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन द वेस्टर्न घाट्स. एक ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, नैटॉ रिसोर रेस (2019): पृ.1-19. http://doi.org/10.1007/s11o53-09588-0
- रामाचंद्रा. टीवी.और भारत एस. (2019 बी) ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन थ्रू कार्बन सेक्वेस्टरिंग इन द सेंट्रल इन द सेट्रल वेस्टर्न घाट्स। रिमोट सेंसिंग इन अर्थ सिस्टम साइंसेज। https://doi.org/10.1007/s41976-019-0010-z
- रामाचन्द्रा, टीवी.,विनय एस, भारत एस. शाशिशंकर ए, (2018 ए) इकोहाइड्रोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ द रिवर बेसिन इन वेस्टर्न घाट्स, वाईजेवीएमः येल जर्नल ऑफ बायोलाजी एंड मेडिसिन (इश्यू फोकसः इकोलाजी एंड इवॉल्यूशन) 91 (2018), पीपी 431-444
- रामाचन्द्रा, टीवी. और भारत एस., गुप्ता एन., (2018 बी). मॉडलिंग लैंडस्केप डायनामिक्स विथ एलएसटी इ प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटक। जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट, 206. 1235-1262, https://doi.org/101016/j.jenvman.2017.08.001
- रामाचन्द्रा, टीवी., भारत, एच.ए, और श्रीजित के. (2015)। जीएचही फुटप्रिंट ऑफ मेजर सिटीज इन इंडिया। रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिव्यूज, 44, 473-495, https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.12.0366.रामाचन्द्रा, टीवी., हेगडे, जी., सेत्तूर, बी., और कृष्णदास जी., (2014)। बायोएनर्जीछ ए सस्टेनेबल एनर्जी ऑप्शन फॉर रूरल इंडिया। एडवांसेज इन फारेस्ट्री लैटर्स (एएफएल), 3 (1), 1-15